कथा-सम्राट की कथाओं में ओझल प्रच्छन्न समाज
अमर कथाकार मुंशी प्रेमचंद हिंदी कथा-साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं ! उन्होंने भारतीय समाज के कमजोर, वंचित और शोषित वर्गों की पीड़ा, संघर्ष और आकांक्षाओं को अपनी कहानियों व उपन्यासों में जगह दी ! हालांकि प्रेमचंद ने मुख्य रूप से किसान, मजदूर, दलित आदि वर्गों की दास्तान पेश की, लेकिन उनके साहित्य में यदि महतो (कृषकों) को आदिम जनजाति आदिवासी नहीं मानें, तो उनके रचना-संसार में आदिवासी जीवन के चित्रण की झलक भी देखने को नहीं मिलती है !
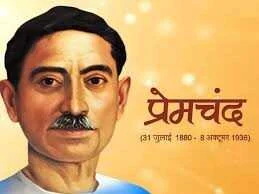
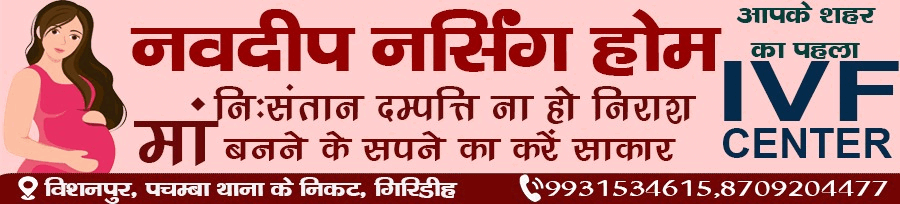

अमर कथाकार मुंशी प्रेमचंद हिंदी कथा-साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं ! उन्होंने भारतीय समाज के कमजोर, वंचित और शोषित वर्गों की पीड़ा, संघर्ष और आकांक्षाओं को अपनी कहानियों व उपन्यासों में जगह दी ! हालांकि प्रेमचंद ने मुख्य रूप से किसान, मजदूर, दलित आदि वर्गों की दास्तान पेश की, लेकिन उनके साहित्य में यदि महतो (कृषकों) को आदिम जनजाति आदिवासी नहीं मानें, तो उनके रचना-संसार में आदिवासी जीवन के चित्रण की झलक भी देखने को नहीं मिलती है !
रंगभूमि, गोदान, ठाकुर का कुंआ, पूस की रात जैसी रचनाओं में ग्रामीण भारत, अछूत, दलित और दबे-कुचले वर्गों की आवाज तो सुनी जा सकती है; परन्तु आदिम जनजातियों – आदिवासियों के जीवन संघर्षों का उल्लेख नहीं मिलता !


अमर कथाकार- प्रेमचंद जी ने सताए, शोषित, वंचित समाज के लोगों के दुःख-दर्द को अपने लेखन का केंद्र बनाया ! कई जगह अछूतों, दलितों, कृषकों की गरीबी, जमींदारों और साहूकारों के अत्याचार तथा उनकी सांस्कृतिक अस्मिता की बातों को संवेदनशीलता के साथ उकेरा है ! प्रेमचंद जी की कथा-संसार रचनाकाल के समय में जनता शोषण, विस्थापन और गरीबी की मार झेल रही थी ! प्रेमचंद इन मुद्दों से गहराई से जुड़े हुए थे और इन वर्गों के साथ सहानुभूति रखते थे ! उन्होंने अपने पात्रों में शोषित, दलित, वंचित समाज की आत्माभिव्यक्ति तथा उनके संघर्ष को जगह दी ! इसे आदिवासी साहित्य की अग्रभूमि या प्रेरणा के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि बाद में उभरे आदिवासी रचनाकारों ने प्रेमचंद से सामाजिक सरोकार और यथार्थ चित्रण की प्रेरणा ली !
बेशक प्रेमचंद जी ने आदिवासी जीवन का जितना चित्रण किया, वह पूर्ण या व्यापक नहीं था, पर उनके सामाजिक दृष्टिकोण और संवेदना ने एक राह दिखाई ! समकालीन आदिवासी साहित्यकारों (जैसे – वंदना टेटे, रमणिका गुप्ता, महाश्वेता देवी, शिवमुर्ति, खोरठा कथाकार- सुधाकर आदि) ने प्रेमचंदीय यथार्थवाद से आगे बढ़कर आदिवासियों की अपनी आवाज, भाषा और संस्कृति को केंद्र में रखा !
मुंशी प्रेमचंद ने प्रत्यक्ष रूप से आदिवासी साहित्य का निर्माण न किया हो, किंतु उनकी कहानियों और उपन्यासों में आदिवासी समाज की झलक, उनका दर्द और सामाजिक अन्याय के प्रति चेतना स्पष्ट दिखती है। उनकी लेखनी ने आदिवासी साहित्य को प्रेरणा, संवेदना और यथार्थवाद की धार दी, जो आगे इस धारा को विस्तार देने वाले साहित्य की नींव बनी !
कथा सम्राट -प्रेमचंद की कहानियों में सीधे “आदिवासी” शब्द या पात्र नहीं मिलते हैं, लेकिन उनकी कुछ कहानियों में गोंड, महतो, गड़ेरिया जैसी समुदायों और समाज के दबे-कुचले, पिछड़े वर्गों का चित्रण मिलता है, जो लगभग आदिवासी जीवन, समस्याओं या उनकी संवेदना से जुड़े हैं !
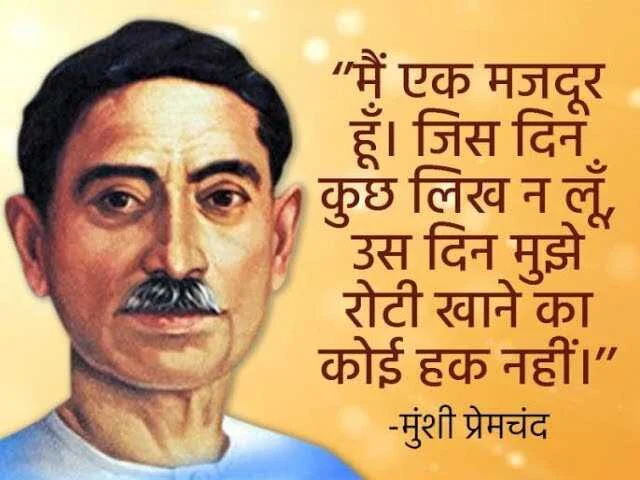
‘विध्वंस’ कहानी में केवल एक “गोंड़िन” पात्र (भुनगी) है, जिसका घर गाँव के पंडित तोड़ देते हैं—यह गोंड आदिवासी समुदाय की ओर इशारा करता है ! ‘मुक्ति मार्ग’ और ‘अलग्योझा’ में झींगुर महतो, बुद्धू गड़ेरिया जैसे चरित्र हैं, जो किसान–पशुपालक और ग्रामीण, कथित आदिवासी या पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं ! उपन्यास ‘रंगभूमि’ में संपूर्णानंद (सुजा) और उसका समाज, शायद आदिवासी वंचना, विस्थापन और संघर्ष का चित्रण करता है !
सीधे-सीधे “आदिवासी”शब्दों का उपयोग प्रेमचंद की भाषा में नहीं दिखता है, लेकिन उनकी कहानियों में गोंड, महतो, गड़ेरिया जैसे पात्र आदिवासी समाज या उसके करीब के समुदायों की ज़िंदगी और पीड़ा को बखूबी दिखाते हैं !
आज का समय प्रेमचंद के समय से काफ़ी बदल गया है ! अपने देश की सामाजिक , शैक्षिक , और आर्थिक स्थिति वर्तमान में इस स्थान पर पहुंच गई है कि वर्तमान शासक वर्ग के साथ मध्य वर्ग के सम्पूर्ण स्वार्थों की सिद्धि मुश्किल है ! हां,, साम्प्रदायिकता, जातिवाद जैसी कुछ समस्याओं से देशी मानसिकता में कुछ अकबकाहट है; फिर भी एक वर्ग विशेष अब महसूस करने लगा है कि उसके सम्पूर्ण संभव-विकास और पूर्णकालिक स्वच्छंदता के लिए राजसत्ता के वर्तमान चरित्र और स्वरुप में बदलाव आवश्यक है ! वर्ग विशेष के इस सोच को स्थायी भाव में रुपांतरित करना आज के समय की सबसे बड़ी मांग और चुनौती बन रही है ! चिंतन का स्वभावांतरण शुद्ध सांस्कृतिक कर्म है, जिसे साहित्य और कला कर्म के द्वारा धार दिया जा सकता है !
इस देश में परिवर्तनकामी जनसंघर्ष का यह दुर्भाग्य रहा है कि इसे साहित्य और संस्कृति के मोर्चे पर प्रेमचंद जी के बाद प्रेमचंद जी जैसा विराट दृष्टिफलक वाला कोई रचनाकर नहीं मिला !
अंग्रेजी राज से पराधीनता तो मिटी लेकिन औपनिवेशिक शोषण , उत्पीड़न नहीं मिटा ! ओद्यौगिकीकरण के कारण जो शहरीकरण हुआ और मजदूरों के वर्ग की जो गोलबन्दी हुई उससे समाज के ढांचे में एक बदलाव आया , जिससे नये अर्थ- सम्बन्ध का विकास हुआ ! लेकिन इस गोलबन्दी और नये सम्बन्धों की सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन में जो भूमिका होनी चाहिए थी , वह नहीं हो सकी ! और न ही इस पूरी प्रक्रिया की समेकित सांस्कृतिक अभिव्यक्ति ही घटित हो हुई ! क्योंकि यदि ऐसा हुआ होता तो समाज में आज जो ” एक नया लम्पट वर्ग ” दिखाई देता है , वह नहीं दिखता ! इसके साथ ही मध्यवर्ग भी इतना कुंठित,स्वार्थी , महत्वाकांक्षी और आत्मकेन्द्रित नहीं हुआ होता ! इससे प्रेमचंद के साहित्यिक संघर्ष का कितना क्षय हुआ है – यह कल्पना से भी परे है ; क्योंकि प्रेमचंद जी के कहे अनुसार ही- “अगर ‘साहित्य राजनीति के आगे मशाल लेकर चलने वाली सच्चाई है ‘ तो इस सच्चाई को परिवर्तनकारी भूमिका में उठकर खड़ा होने का इससे अच्छा समय आखिर और कैसा होगा ? इसलिए प्रेमचंद की परंपरा में खड़े रचनाकारों को आज अपनी विरासत से सबक सीखते हुए अपनी भूमिका में खड़े होने की आवश्यकता है !
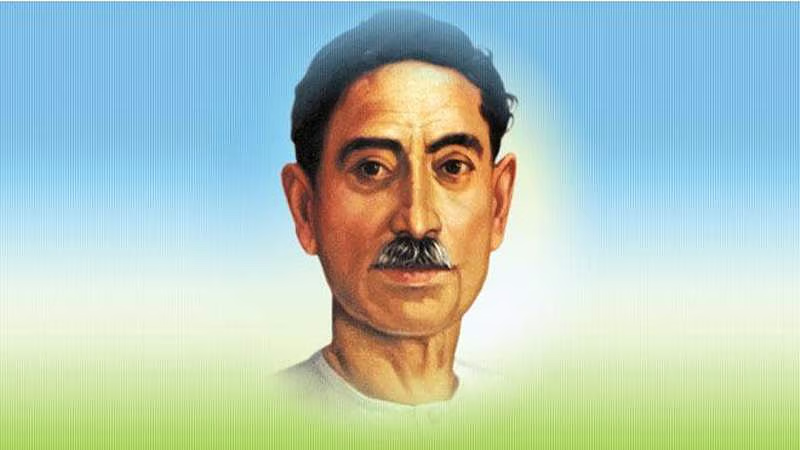
मेरी समझ से प्रेमचंद जी के कथा संसार में यथार्थ का जो त्रासद रुप उद्घाटित हुआ है, उसके दो ही प्रमुख कारक तत्व दिखते हैं – पहला -औपनिवेशिक शोषण- दमन, और दूसरा – इस देश के ही सुविधाभोगी दलाल और महत्वाकांक्षी मध्य वर्ग !
धर्म और अंधविश्वास/ साम्प्रदायिकता/ जातिय विद्वेष/ स्त्रियों पर अत्याचार/ निरंकुश नौकरशाह/ रुढ़ीवादी और जनद्रोही जनप्रतिनीधि गठबंधन/ कुंठित, दलाल मध्यवर्ग की अकर्मण्यता और महत्वाकांक्षा आदि पर प्रहार करने में प्रेमचंद “अग्रधर्मा” थे ! प्रेमचंद जी की सभी कहानियां अपने समय और समाज की दहकती और वास्तविकता की बेचैन अभिव्यक्ति हैं , इसमें कोई संदेह नहीं ! ऐसी अभिव्यक्ति ,जिनमें यथार्थ जितना विद्रूप और अमानवीय है, उतना ही सशक्त तीव्र प्रहारक है, उसके ध्वंस और निर्माण का सांस्कृतिक संदेश भी !
प्रेमचंद जी की प्रासंगिकता के परिप्रेक्ष्य में उनकी कहानियों के प्रमाणों और तथ्यों की विवेचना अब तक हजारों- हजार बार हो चुकी होंगी ऐसा मेरा ख़याल है ! वस्तुत: सत्य तो यह है कि प्रेमचंद सत्य से कहीं पीछा नहीं छुड़ाते ! और फिर जिस कालावधि में प्रेमचंद जी ने कहानियों की रचना की है , उस समय की स्थितियां वैसी ही रही होंगी ! यह बात उनकी परवर्ती और तथाकथित रुप से यथार्थवादी कही जाने वाली कहानियों पर ही लागू नहीं होती , बल्कि उनकी आदर्शवादी कही जाने वाली कहानियों पर भी लागू होती हैं , परन्तु – यह भी सत्य और आश्चर्य का विषय है , कि देश का (झारखण्ड का) आदिवासी समुदाय वन प्रान्तर की ओट में प्रच्छन्न तो था ही , देश के इतने बड़े कथा-सम्राट की दृष्टि से ओझल और कलम से भी अछूता ही रह गया !
नोट – इस आलेख में प्रेमचंद और उनके साहित्य को लेकर जो विचार हैं, वे पूर्ण रूप से आलेख के लेखक महेन्द्रनाथ गोस्वामी “सुधाकर” जी के अपने विचार हैं.


Comments are closed.